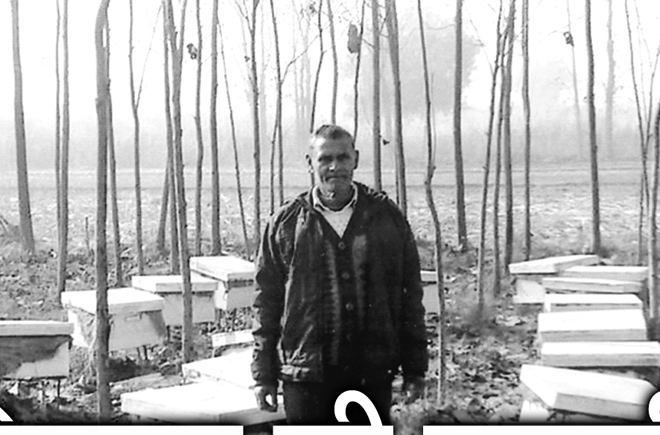कपास यानी नरमा को?भारत में ‘सफेद सोना’ भी कहा जाता?है. लेकिन पिछले साल हरियाणा और पंजाब राज्यों में इस सफेद सोने पर सफेद मक्खी ने जम कर कहर बरपाया था. जिस से यह ‘सफेद सोना’ न रह कर ‘खोटा सोना’ बन गई थी और किसानों को हजारोंलाखों रुपए की चपत लगी थी. सरकार को करोड़ों रुपए मुआवजे के तौर पर जारी करने पड़े थे. पिछली बार अनेक बीज कंपनियों व कीटनाशक कंपनियों के सारे दावे धरे रह गए और नरमा फसल पर सफेद मक्खी के प्रकोप को अनेक तरह के कीटनाशक भी नहीं रोक पाए. इस बार इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख कर पंजाब सरकार ने सफेद मक्खी के काले साए से नरमा फसल को बचाने के लिए ‘वार प्लान’ तैयार किया है. इस योजना के तहत कपास की खेती में माहिर कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों की टीमें तैनात की जाएंगी. टीमों में 200 से ज्यादा जानकार लोग होंगे, जो समयसमय पर नरमा फसल का मुआयना करेंगे.
हरियाणा सरकार ने पिछले साल सफेद मक्खी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अब जा कर 967 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी किया है, जो किसानों के बैंक खातों में सीधा जाएगा.दूसरी तरफ धोखा खा चुके किसानों ने भी कमर कस ली है. कपास बोने वाले किसानों का कहना है कि हम नरमा फसल में उत्पादन के लिए बीज की अच्छी किस्म से ले कर बीजाई के खास तरीके अपनाएंगे और समयमसय पर जानकारों से सलाहमशवरा भी करेंगे. कृषि जानकारों का मानना है कि नरमा की अच्छी पैदावार के लिए खेत में नरमा पौधों की सही संख्या होना और सिंचाई का सही इंतजाम होना जरूरी है. नरमा पौधों की सही संख्या के बाद पौधों के लिए सही मात्रा में खाद व पानी की जरूरत होती है. उस के अलावा खास बात लंबी अवधि तक फल देने वाले बीज का चुनाव भी है.
प्रगतिशील किसानों का कहना है कि 1 एकड़ में नरमा के 4 हजार से 4800 तकपौधे होने चाहिए. पौधों के बीच में 3 से सवा 3 फुट तक का फासला होना चाहिए, ताकि पौधों को बढ़ने के लिए सही जगह मिले और पौधों के बीच में सही फासला होने पर पौधों को हवा धूप ठीक से मिले, जिस से उन में फुटाव ठीक होगा.माहिरों का कहना?है मौसम के मिजाज का कुछ पता नहीं चलता, इसलिए नरमा की बोआई सीधी न कर के डोलियों (मेंड़ों) पर करें. अगर किसान हाथ से बोआई करते?हैं, तो बीज के साथ गोबर की खाद जरूर डालें.
आज ज्यादातर किसान देशी कपास न बो कर बीटी कपास की ही बीजाई करते?हैं. बीटी कपास के लिए किसानों को यह?भी जानना जरूरी?है कि उस के लिए ज्यादा खुराक चाहिए. इस की बीजाई के दौरान 1 एकड़ में 20 किलोग्राम पोटाश, एक बैग डीएपी, 20 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट जरूर डालें.कुछ क्षेत्रों में जहां खारा पानी है, वहां 1 एकड़ में कम से कम 8 से 10 ट्राली प्रति एकड़ गोबर की खाद खेत तैयार करते समय जरूर डालें, क्योंकि नरमा में पौधे ज्यादा नमक सहन नहीं कर पाते और गोबर की खाद डालने से उन्हें ताकत मिलती है.
अंगरेजी में एक कहावत है ‘वैल बिगेन इज हाफ डन’ यानी किसी काम की अगर शुरुआत अच्छी हो तो समझ लो कि आधा काम निबट गया. यह बात खेती में भी लागू होती है. खेती की शुरुआत बीज से होती है. बीज ही खेती का मुख्य आधार है. बीज पर ही फसलों का उत्पादन टिका होता है. अच्छे बीज जहां औसतन 20 से 30 फीसदी ज्यादा पैदावार देते हैं. वहीं खराब बीजों से मेहनत, पैसा और समय दोनों बरबाद हो जाते हैं.
अच्छी शुरुआत अच्छे बीजों के साथ
डाक्टर बीज : ‘हर हाल में खुशहाल डाक्टर बीज का यही कमाल’? यह नारा है डाक्टर बीज उत्पादन करने वाली कंपनी सोलार एग्रोटैक का. कंपनी का 2 तरह का कपास बीज बाजार में है.
सोलार 65 : मध्यम अवधि, 155-160 दिनों तक फसल तैयार होने का समय. पौधे सीधी बढ़त वाले एक समान बड़े और वजनदार टिंडे.
नरमा का खिलाव अच्छा चुगाई आसान. अधिक टिंडे. रस चूषक कीटों के प्रति सहनशील. पौधों की लंबाई 150 से 160 सेंटीमीटर. बीजाई का समय 31 मई तक. रेशे की लंबाई 29 से 30 मिलीमीटर. सभी प्रकार की नरमा उगाने वाली मिट्टी के लिए सही है.
‘सोलार 65’ को हरियाणा के हिसार क्षेत्र के अनेक किसानों ने आजमाया है, जिन में किसान साधुराम (मो. नं. 0881300016), अजीत सिंह (मो. नं. 9813244409), सतनाम सिंह (मो. नं. 9896274777) जैसे अनेक किसान हैं, जिन्होंने इस बीज को बोया था और अच्छी पैदावार ली.
जींद के किसान सुभाष (मो. नं. 8607520822), जगदीश (मो. नं. 9728897165) और फतेहाबाद के किसान सुनील कुमार (मो. नं. 9992115136) ने भी इस बीज से अच्छी पैदावार ली.
गोल्ड स्टार : मध्यम अवधि 160-165 दिनों में तैयार होने वाली फसल. पौधे सीधी बढ़त वाले. मजबूत तना. हर तरह के मौसम में कामयाब पौधे की लंबाई 6 से 7 फुट. पौधे की ऊंचाई जल्दी बढ़ती है. टिंडे पासपास और ज्यादा संख्या में मिलते हैं. टिंडे मोटे व वजनदार तकरीबन 5 से 5.6 ग्राम. पौधों की संख्या ज्यादा और अच्छी पैदावार. खिलाव अच्छा चुगाई भी आसान. रस चूसक कीटों के प्रति सहनशील. हर प्रकार की नरमा लगाने वाली मिट्टी में कामयाब.
इस गोल्ड स्टार नरमा बीज को जिला फतेहाबाद हरियाण के किसान राकेश (मो. नं. 9802656653), जींद के किसान जगवीर (मो. नं. 9467037975), रोहतक के किसान मनजीत (मो. नं. 9813468762) व हिसार के किसान मोहित (मो. नं. 9416672767) ने बोया और इस बीज से अच्छी फसल ली है.
शिल्पा व कार्तिक : कपास की उन्नत किस्मों में शिल्पा और कार्तिक भी शामिल है. इन में मरोडिया नामक बीमारी से छुटकारा मिल जाता है. इन दोनों किस्मों में फल झड़ने के बाद?भी अंकुरण होता है. इन में विपरीत परिस्थितियों में जूझने की कूवत भी है.फसल मई के आखिरी महीने तक बोई जा सकती है और पकने की अवधि 155 से 160 दिन है. बीज कंपनी का कहना?है कि यह किस्म कम पानी में भी अच्छी बढ़त देती है. इन किस्मों में बड़ा टिंडा होता है और रस चूसक कीटों का हमला कम होता?है. यह लीफकर्ल बीमारी के प्रति सहनशील है.
विक्रम 310 : इस के टिंडे मध्यम आकार के होते हैं. फसल तैयार होने का समय 160-170 दिन है. इस किस्म की बोआई मई के आखिर तक होती है. सामान्य नरमे की तुलना में कम दूरी पर बोया जाता है.
दक्ष सी 111 : टाटा कंपनी के दक्ष सी 111 बीज की खासीयत के बारे में बीज कंपनी का कहना है कि इस के टिंडे बड़े साइज के व अधिक मात्रा में आते हैं.
फसल पकने तक हरी रहती है व पौधे की टहनियों में लचक होने के कारण नरमा चुनते समय पौधा टूटता नहीं है. रस चूसक कीटों के प्रकोप में कमी होती है. फसल पकने की अवधि 155-165 दिन है. पौधों की लंबाई 5.5 से 6 फुट तक होती है. बोआई मई के आखिर तक कर सकते हैं.
राघव, बलवान, एनसीएस 9013 : नुजिवीडू सीड्स लि. की एनसीएस-9013, राघव व बलवान जैसी वैराइटी हैं, जिन्हें हरियाणा व पंजाब में किसानों ने आजमाया?है और अच्छी पैदावार ली है. देखें संबंधित बौक्स (इन्होंने आजमाया)
सिकंदर टाटा : कैमिकल्स का धान्या संकट नरमा ‘सिकंदर’ भी बीज के विश्वास और मुनाफे का प्रतीक है. इस की खास विशेषताएं हैं मध्यम पछेती पकने वाली फसल, अधिक टिंडे व बढि़या खिलाव, रस चूषक कीटों के प्रति बेहतर सहनशील, लंबे व मजबूत आकार का पौधा.
यह बीज उत्तम भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है. इसे सैकड़ों किसानों द्वारा आजमाया गया?है और तकरीबन 10 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार भी ली है.
सुपर श्रद्धा : सुपर सीड्स कंपनी का सुपर श्रद्धा संशोधित देशी कपास बीज है. फसल पकने का समय 155-160 दिन है और फसल बीजाई का समय अप्रैल से जून महीने तक है. यह किस्म सिंचित व असिंचित दोनों क्षेत्रों के लिए सही है और इसे हर प्रकार की जमीन में पैदा कर सकते हैं.
सुपर 931 : इस पौधे का ऊंचा कद, मोटे टिंडे होते हैं व पूरी पैदावार मिलती है. फसल पकने का समय 160-165 दिन है व टिंडों का वजन 5 से साढ़े 5 ग्राम होता है. इस के रोएंदार पत्ते होते हैं. यह रसचूसक कीट के लिए प्रतिरोधक व सिंचित व असिंचित दोनों क्षेत्रों के लिए सही है.
कावेरी बुलेट व कावेरी जादू : कावेरी बुलेट में फसल पकने का समय 145 से 150 दिन है. इस में 2 से 3 फल शाखाएं व 21 से 24 तक उपफल शाखाएं निकलती हैं. फूल आने की अवधि 40 से 45 दिन है.
कावेरी जादू में फसल पकने की अवधि 150-160 दिन है. पौधों को पासपास बोने के लिए सही बीज, अधिक टिंडे लगते हैं. सभी तरह के हालात के अनुकूल हैं. सूखा सहने की क्षमता है और रसचूसक कीट के लिए प्रतिरोधक है. इस पौधे की ऊंचाई 5 से 5.5 फुट होने पर ही टिंडों को तोड़ना सही रहता है. इस के अलावा अंकुर 3228, अंकुर 3028, अंकुर 3244 , जेके 0109, जेके 8940 जैसी अनेक वैराइटियां हैं, इसलिए किसान बीज बोने से पहले अपने इलाके के आधार पर सही बीज का चुनाव करें और संबंधित जानकारी ले कर बीज जरूर बोएं. कंपनी के वादों से पहले पड़ताल भी जरूरी है.
मशीन से भी बोआई
पशुचालित प्लांटर: केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल द्वारा बनाई गई पशुओं से चलने वाली बोआई मशीन से भी कपास की बोआई की जाती है. इस पशुचालित प्लांटर से कतार से कतार की दूरी व बीज से बीज की दूरी नियंत्रित की जाती है. चूंकि कपास का बीज महंगा होता है, इसलिए इस मशीन से बोने पर बीज की बरबादी नहीं होती.
इस मशीन से सरसों जैसे छोटे बीज से ले कर मध्यम और बड़े बीज जैसे सोयाबीन मूंगफली, मक्का आदि की भी बोआई की जा सकती है. इस मशीन के लिए केवल 1 जोड़ी बैलों की जरूरत होती है, जो मशीन को खींच कर चलाते हैं. मशीन की अनुमानित कीमत 15 हजार रुपए है.
इस मशीन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए किसान केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल के नंबरों 0755-2521133, 2521139 व 2521142 पर बात कर सकते हैं.
स्वचलित सीड ड्रिल मशीन : हाथ से चलने वाली सीड ड्रिल मशीन और ट्रैक्टर के साथ जोड़ कर चलने वाली आटोमैटिक सीड ड्रिल मशीन से भी कपास की बिजाई कर सकते हैं. इस के लिए भारत एग्रो इंजीनियरिंग की मशीनें उपलब्ध हैं, जिन पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है. इन मशीनों से संबंधित जानकारी के लिए कंपनी के फोन नंबर 02827-253858पर बात कर सकते हैं.
हरियाणा के किसानों ने जो आजमाया
दक्ष सी 111 का इस्तेमाल करने वाले किसान
नाम : राजेंद्र सिंह
गांव : नहला
जिला : फतेहाबाद
मो. नं.: 9468022282
पैदावार : 27 मन प्रति एकड़
नाम : हिम्मत सिंह
गांव : संडौल
जिला : हिसार
मो. नं.: 9050441556
पैदावार : 30 मन प्रति एकड़
नाम : सुंदर सिंह
गांव : पावड़ा
जिला : हिसार
मो. नं.: 9992231031
पैदावार : 32 मन प्रति एकड़
नाम : धर्मवीर सिंह
गांव : हांसावाला
जिला : हिसार
मो. नं.: 9050861225
पैदावार : 20 मन प्रति एकड़
नाम : अनिल कुमार
गांव : छान
जिला : हिसार
मो. नं.: 9467244657
पैदावार : 29 मन प्रति एकड़
नाम : सतपाल
गांव : बधावड़
जिला : हिसार
मो.नं.: 8529481875
पैदावार : 28 मन प्रति एकड़
नाम : रणदीप सिंह
गांव : खरक पुनिया
जिला : हिसार
मो. नं.: 9966577443
पैदावार : 33 मन प्रति एकड़
बलवान/एनसीएस 9013 का
इस्तेमाल करने वाले किसान
नाम : राजेंद्र
गांव : शिमला, कलायत
मो. नं.: 08930112385
नरमा : बलवान
पैदावार : 25 मन प्रति एकड़
नाम : रामेश्वर
गांव : कालता, जींद
मो. नं.: 09466690759
नरमा : बलवान
पैदावार : 25 मन प्रति एकड़
नाम : सुरेश
गांव : कुचराना कलां
मो. नं.: 09991198433
नरमा : बलवान
पैदावार : 28 मन प्रति एकड़
नाम : संजय
गांव : पौली, जुलाना, जींद
मो. नं.: 08529856800
नरमा : बलवान
पैदावार : 30 मन प्रति एकड़
नाम : ओमप्रकाश
गांव : सैंथली, नरवाना
मो. नं.: 09467238216
नरमा : एनसीएस 9013
पैदावार : 30 मन प्रति एकड़
नाम : मनमोहन लाडी
गांव : कालता, उचाना
मो. नं.: 09416485370
नरमा : बलवान
पैदावार : 34 मन प्रति एकड़
नाम : नाथूराम
गांव : बाणा, नरवाना
मो. नं.: 09729263403
नरमा : बलवान
पैदावार : 32 मन प्रति एकड़
धान्या संकर, नरमा सिकंदर
इस्तेमाल करने वाले किसान
नाम : कृष्ण कुमार
गांव : रावल वास
जिला : हिसार
मो. नं.: 9812674587
पैदावार : 10.40 क्विंटल प्रति एकड़
नाम : चंद्रभान
गांव : देवां
जिला : हिसार
मो. नं.: 9467297446
पैदावार : 8 क्विंटल प्रति एकड़
नाम : भूप सिंह फोगट
गांव : सिघरान
जिला : हिसार
मो. नं.: 9466282080
पैदावार : 9 क्विंटल प्रति एकड़
नाम : अशोक
गांव : संगतपुरी
जिला : जींद
मो. नं.: 9992707851
पैदावार : 30 मन प्रति एकड़
नाम : पप्पू
गांव : भौगंरा
जिला : जींद
मो. नं.: 9896212587
पैदावार : 32 मन प्रति एकड़
नाम : लीजाराम
गांव : डुंडवा
जिला : कैथल
मो. नं.: 989635596
पैदावार : 30 मन प्रति एकड़
नाम : छज्जूराम
गांव : ठाणी शंकर
जिला : भिवानी
मो. नं.: 9992061237
पैदावार : 7.5 क्विंटल प्रति एकड़